सूचना का अधिकार पर निबंध Essay Right to Information
सूचना का अधिकार पर निबंध Essay on Right to Information
हैलो नमस्कार दोस्तों आपका बहुत - बहुत स्वागत है इस लेख इस लेख सूचना का अधिकार पर निबंध (Essay on Right to Information) में।
दोस्तों इस लेख में आज हम सूचना का अधिकार पर निबंध पड़ेंगे, जिसमें आपको इस अधिनियम के बारे में समझाया गया है।
यह निबंध कक्षा 5से 12वीं तथा उच्च कक्षाओं में अक्सर पूँछा जाता है, तो आइये शुरू करते है, यह लेख सूचना का अधिकार पर निबंध:-
इसे भी पढ़े:- भारतीय संविधान पर निबंध
सूचना का अधिकार क्या है what is Right to Information
भारत देश एक प्रजातांत्रिक देश (Democretic Country) है इसमें जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता की सरकार होती है अर्थात कहा जा सकता है,
कि लोकतांत्रिक देश में जनता ही देश की मालिक होती है, इसीलिए मालिक होने के साथ ही जनता को देश में होने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी होता है,
कियोकि जो सरकार जनता ने चुनी है, वह देश के बाहर तथा देश के भीतर क्या कैसे और कहां कार्य कर रही है? क्योंकि देश की जनता ही विभिन्न प्रकार के टैक्स देती है, जिनसे देश की सरकार चलती है
और देश के विकास में उस पैसे को खर्च किया जाता है, इसीलिए जनता को सरकार से जुड़ी सभी बातों को जानने का अधिकार ही सूचना का अधिकार (Right to Information) कहलाता है।
साधारण भाषा में कहें कि जनता के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है, वह सरकार देश के विकास में विभिन्न प्रकार के कार्य करती है,
उन कार्यों के विकास, व्यय, सफलता आदि से सम्बंधित सूचनाओं को किसी भी माध्यम (प्रिंट मीडिया, सीडी, ईमेल आदि) प्राप्त करना सूचना का अधिकार (Right to information) कहलाता है, जो एक मौलिक अधिकार है और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकारों का हिस्सा है।
सूचना का अधिकार कब लागू हुआ When did the right to information come into force
भारत के नागरिकों में बोलने की अभिव्यक्ति का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए, शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही लोक प्राधिकारीयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समस्त सूचनाओं
को समय - समय पर आसानी से नागरिकों तक पहुँचाने के उद्देश्य से देश की संसद ने एक कानून पारित किया, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI 2005) कहा गया। सूचना का अधिकार
अधिनयम का इतिहास 2002 से शुरू हुआ था, जब भारत सरकार की संसद में 2002 को सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम को पारित किया गया
और इस अधिनियम को जनवरी 2003 में राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी भी मिल गई किन्तु इसकी नियमावली बनाने के नाम पर इसे लागू नहीं किया गया।
इसके बाद प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार ने पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था लाने के लिए एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज और देश बनाने के लिए 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम संसद
में पारित किया गया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और यह 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू हो गया और सूचना की स्वतंत्रता का विधेयक 2002 को निरस्त
कर दिया गया। सूचना के अधिकार अधिनियम में इस प्रकार की व्यवस्था की गई, कि आम जनता सरकार से किस प्रकार विभिन्न उद्देश्यों, विकास कार्यों की जानकारियाँ प्राप्त करेगी और सरकार किस प्रकार से जनता के किए गए सवालों का जवाब देगी।
सूचना का अधिकार के प्रावधान Right to Information Provisions
- सूचना के अधिकार अधिनियम में लोक प्राधिकारियों को यह निर्देश दिए गए, कि वह 30 दिन के भीतर जनता द्वारा विभिन्न विकास के कार्यों तथा अन्य सूचनाओं जो इस अधिनियम के दायरे में आती हों से संबंधित मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराएँ यदि वह सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित होती हो तो 48 घंटे के अंदर सूचना सम्बंधित व्यक्ति को उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।
- यदि लोक अधिकारी से कोई सूचना माँगी जाये अगर वे निर्धारित समय में कोई भी सूचना जनता को प्रदान नहीं करते हैं या फिर जो विषय वस्तु सूचना जनता को प्राप्त होती है, जनता उससे असंतुष्ट हैं, तो वे राज्य के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग और केंद्र के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग में अपील भी कर सकते हैं।
- इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्र की संप्रभुता एकता अखंडता सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली विभिन्न सूचनाएँ प्रकट करने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गई है।
- इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक निकायों व उनसे सम्बंधित पदों को भी इस अधिनियम के दायरे में लाया गया है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्त सदस्यों की नियुक्ति होगी, जिनसे मिलकर एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा, जबकि राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार से एक राज्य सूचना आयोग का भी गठन होगा।
सूचना का अधिकार अधिनियम की उपलब्धियाँ Achievements of Right to Information Act
- सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा मंत्रियों द्वारा जो विदेश यात्रा की जाती है, उस विदेश यात्रा पर जो खर्च होता है, जो व्यय होता है, उसको सार्वजनिक करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त की है। इसके द्वारा जो मंत्री फालतू में विदेश यात्रा करते है, तो उन पर विदेश यात्रा न करने का दबाव बनाया जा सकता, जिससे सरकारी व्यय अधिक ना हो।
- सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा ही विभिन्न बड़े बड़े पदाधिकारियों जैसे कि मंत्री, नौकरशाहों ,न्यायाधीशों की संपत्तियों की जानकारी भी प्राप्त होती है। इसके प्रभाव के चलते अब नौकरशाहों द्वारा अपनी परिसंपत्तियों को सरकारी वेबसाइट पर दिखाया जाने लगा है। साथ ही वार्षिक स्तर पर इसका अघटन भी किया जाता है।
- इस अधिनियम के द्वारा देश में होने वाले विभिन्न प्रकार की परीक्षा उनके परिणामों और परीक्षाओं से संबंधित जानकारियों को उद्घाटित करने के लिए संबंधित संस्थाओं पर दबाव डाला है, जिससे जनता को सटीक और सरल रूप से जानकारी प्राप्त हो जाती हैं।
- केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देशों के फलस्वरूप आरटीआई के आवेदनों के फलस्वरुप सरकार ने 2012 में आरटीआई एक्ट (RTI act 2005) के तहत फाइल नोटिंग को उपलब्ध कराया है, इससे नौकरशाहों पर यह दबाव पड़ता है, कि वह फाइलों पर उचित तरीके से लिखें।
- सूचना के अधिकार अधिनियम संबंधी आवेदनों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के घोटाले भी सामने आए हैं, इसमें आदर्श आवासीय घोटाला, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला आदि शामिल है।
आरटीआई के उद्देश्य और लाभ Object and Benefits of RTI
आरटीआई कानून का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी दफ्तरों में जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है, जिससे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जैसी बुराई पर रोक लगाई जा सके और भारतीय नागरिक अपना काम ठीक समय पर करवा सकें।
इसके लिए भारत सरकार ने केंद्र स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना भी की है और साथ में ही राज्य सूचना आयोग की भी स्थापना की है।
सूचना के अधिकार अधिनियम में बताया गया, कि ऐसी कोई भी जानकारी जो संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों को दी जा सकती है, वह जानकारी आम नागरिकों को भी दी जा सकती है।
इसके आलावा लगभग 22 विषयों को (डिफेन्स, गुप्त विभाग आदि) छोड़कर अन्य विषयों से सम्बंधित जानकारी प्राप्त कर सकते है।
इस कानून के तहत स्कूल में गैरहाजिर होने वाले स्टाफ की जानकारी, सरकारी अस्पतालों में गैरहाजिर डॉक्टर और रिश्वतखोरी की जानकारी, दवाइयाँ ना होना
उनकी जानकारी, राशन दुकान पर राशन उपलब्ध ना हो इसकी जानकारी के साथ अन्य जानकारी आप आरटीआई (RTI) के तहत प्राप्त कर सकते हैं।
इसके लिए भारत सरकार ने पब्लिक इनफॉरमेशन ऑफीसर (Public Information Officer) की नियुक्ति की है, जो सभी सरकारी विभागों से सम्बंधित सभी सूचनाएँ आम नागरिकों को उपलब्ध कराता है।
सूचना के अधिकार अधिनियम के समक्ष चुनौतियाँ Challenges before the Right to Information Act
सूचना के अधिकार अधिनियम के अस्तित्व में आ जाने के बाद सबसे बड़ा खतरा आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए हो गया है, इन्हें कई तरीकों से उत्पीड़ित और प्रताड़ित किया जाने लगा है।
औपनिवेशिक हितों के अनुरूप बना 1923 का अधिकारिक गोपनीयता अधिनियम आरटीआई की राह में प्रमुख रोड़ा बना हुआ है।
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस अधिनियम को खत्म करने की सिफारिश भी की है, जिस पर पारदर्शिता के लिहाज से अमल आवश्यक है। इसके अलावा कुछ अन्य चुनौतियाँ भी हैं
जैसे कि नौकरशाही में अभिलेखों के रखने व उनके संरक्षण की व्यवस्था बहुत कमजोर है। सूचना आयोगों को चलाने के लिए पर्याप्त अवसर रचना और स्टाफ का अभाव भी मुख्य कारण है।
सूचना के अधिकार कानून के कारण अन्य कानून जैसे विसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम का कुशल क्रियान्वयन नहीं हो पाया है।
उपसंहार Conclusion
सूचना का अधिकार अधिनियम आज विश्व के लगभग 80 से अधिक देशों में लागू हो चुका है, इन देशों में स्वीडन फ्रांस, कनाडा, मेक्सिको एवं भारत प्रमुख राष्ट्र हैं। आज भारत में राजस्थान से
लेकर मणिपुर तक उत्तर में हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों द्वारा सूचना के अधिकार कानून का प्रयोग किया जा रहा है और यह कानून आगे भी बढ़ रहा है,
लेकिन इस कानून के दायरे व मुख्य प्रावधानों के संबंध में मत मतान्तरो एवं अस्पष्ट क्षेत्रों को भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है,
कि सूचना का अधिकार जन अधिकारों के पक्ष में आगे तो बड़ा है, लेकिन वास्तविक लाभ को प्राप्त करने के लिए इसके मार्ग में आने वाली संरचनात्मक संस्थागत और प्रक्रियागत बाधा जटिलताओं के दुष्चक्र को तोड़ना होगा। इस क्रम में जागरूकता
फैलाने वाला प्रमुख अभियान चलाना होगा। सूचना का अधिकार के संरक्षण में न्यायालयों और सिविल सोसाइटी संगठनों को अग्रणी भूमिका निभानी होगी तभी जाकर यह अधिनियम ठीक प्रकार से क्रियान्वित और सफल हो पाएगा।
दोस्तों यहाँ पर आपने सूचना का अधिकार पर निबंध (Essay on Right to Information) पढ़ा करता आशा करता हूँ, आपको यह लेख अच्छा लगा होगा।
FAQs for RTI
Q.1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 कब लागू हुआ?
Ans. अधिकार अधिनियम 2005 को भारत सरकार के द्वारा 15 जून 2005 को मंजूरी मिल गई और इसे पूरी तरह से सभी धाराओं के साथ 12 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया गया।
Q.2. RTI सबसे पहले कहाँ लागू हुआ?
Ans. सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई सबसे पहले भारत के राज्य तमिलनाडु में 1997 में लागू हो गया था। इसके पश्चात लागू करने वाले राज्य गोवा तथा कर्नाटक है।
Q.3. सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला देश कौन सा है?
Ans. सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला विश्व का सबसे पहला देश स्वीडन है जिसने 1766 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया था।
इसे भी पढ़े:-
- भारत में जल संकट पर निबंध Essay on water crisis in india
- गणतंत्र दिवस के महत्व पर निबंध Essay on importence of republic day
- संविधान दिवस पर निबंध Essay on constitution day
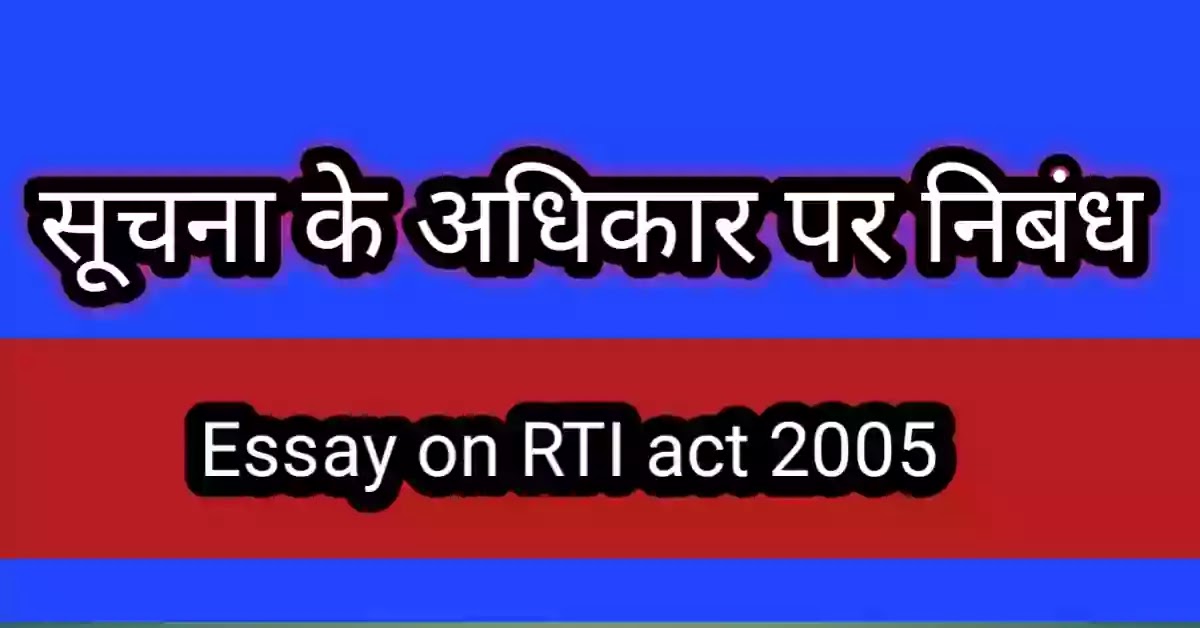

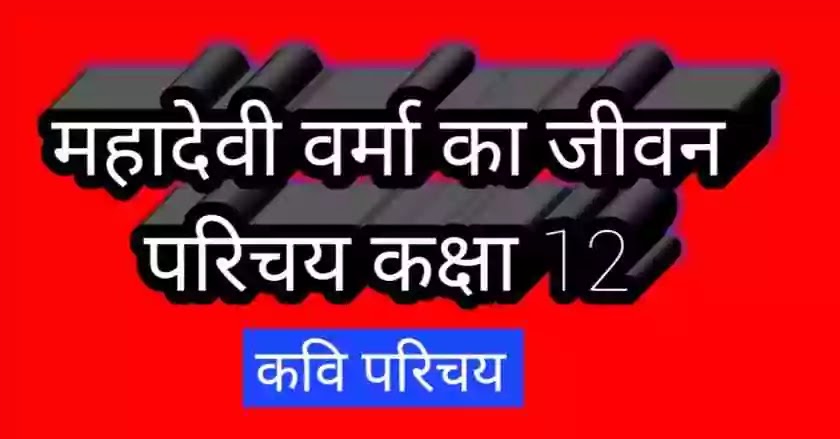


Comments
Post a Comment